Class 12 : हिंदी अनिवार्य – अध्याय 15.श्रम-विभाजन और जाति-प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज
संक्षिप्त लेखक परिचय
🌟 जीवन परिचय
✨ डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ।
✨ वे भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे।
✨ बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता का सामना किया।
✨ उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
🌟 साहित्यिक योगदान
📖 डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के पक्ष में प्रखर लेखन किया।
🖋️ उन्होंने “जाति का विनाश”, “श्रम विभाजन और जाति प्रथा” जैसे महत्त्वपूर्ण निबंध लिखे, जिनमें उन्होंने भारतीय समाज की विषमताओं का विश्लेषण किया।
💡 वे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे और शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन मानते थे।
🎯 उनकी रचनाएँ तर्कपूर्ण, तथ्याधारित और क्रांतिकारी विचारों से भरपूर हैं।
🌏 आंबेडकर का साहित्य और विचारधारा आज भी सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा देता है।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन
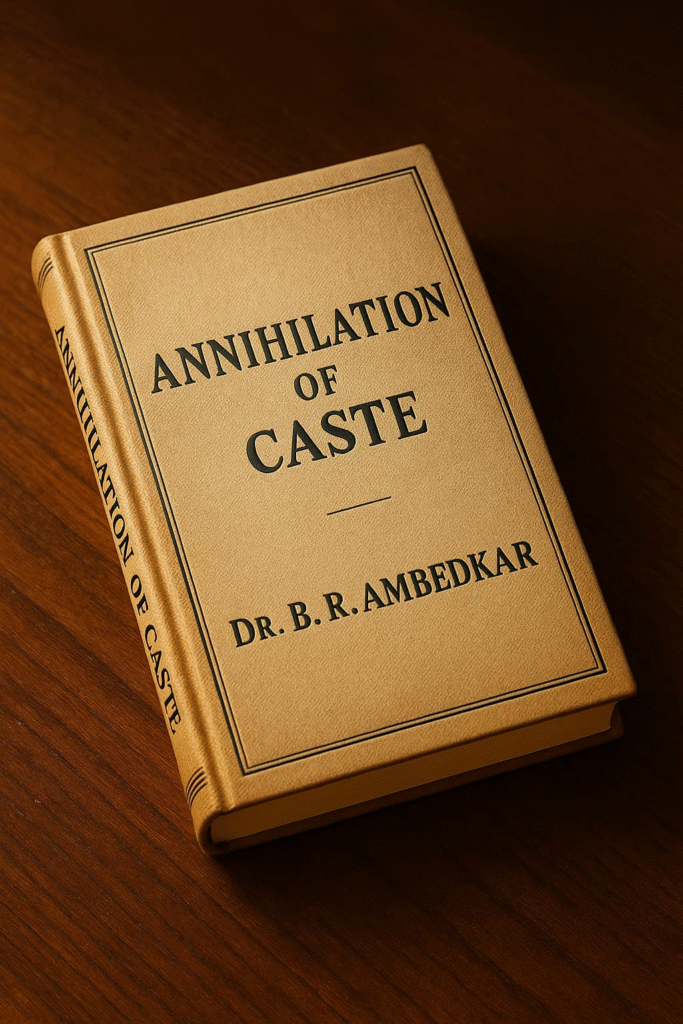
📚 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज – व्याख्या और विवेचन
✨ भूमिका एवं लेखक परिचय
🎂 डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे।
📖 इस निबंध में उन्होंने जाति प्रथा की कमियों को उजागर किया और एक न्यायपूर्ण, समानता-आधारित समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की।
🔍 श्रम विभाजन और जाति प्रथा की आलोचना
⚠️ जाति प्रथा की मूलभूत समस्याएं
श्रमिक विभाजन – यह केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का अस्वाभाविक बंटवारा है।
ऊंच-नीच का भाव – वर्गों के बीच कृत्रिम श्रेष्ठता और हीनता की भावना फैलाती है।
🚫 स्वाभाविकता का अभाव
जाति प्रथा व्यक्ति की रुचि और योग्यता को नजरअंदाज करती है।
पेशे का चुनाव जन्म के आधार पर तय कर देती है।
🔒 पूर्वनिर्धारण की समस्या
माता-पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर गर्भधारण से पहले ही पेशा तय कर दिया जाता है।
📉 आर्थिक हानि और बेरोजगारी
एक ही पेशे में जीवनभर बांध देती है।
पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं, जिससे तकनीकी परिवर्तन के साथ बेरोजगारी बढ़ती है।
🧠 मानसिक प्रभाव
अरुचि और मजबूरी से काम, जिससे कुशलता का अभाव।
कार्य में न मन लगता है, न नवाचार संभव होता है।
🌟 मेरी कल्पना का आदर्श समाज
🪴 रचनात्मक दृष्टिकोण
अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित है।
🔄 गतिशीलता की आवश्यकता
परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक आसानी से पहुंचना चाहिए।
🤝 सामूहिक हितों में भागीदारी
समाज के सभी हितों में सबकी भागीदारी और रक्षा का भाव होना चाहिए।
🥛 लोकतंत्र और भ्रातृत्व
दूध-पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा, जिसमें कोई भेदभाव न हो।
लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि सामूहिक जीवन जीने की रीति है।
🕊️ स्वतंत्रता की व्याख्या
गमना-गमन की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार सबको मिले।
व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आवश्यक, अन्यथा यह दासता का रूप ले लेती है।
⚖️ समता का सिद्धांत
आलोचनाओं के बावजूद समान अवसर सभी को मिलने चाहिए।
व्यक्ति की शक्ति तीन आधारों पर टिकी है:
शारीरिक वंश परंपरा
सामाजिक उत्तराधिकार
व्यक्तिगत प्रयत्न
📌 व्यावहारिक आवश्यकता
राजनेता को समान व्यवहार का नियम अपनाना चाहिए क्योंकि सबके लिए अलग मूल्यांकन संभव नहीं।
मानवता का वर्गीकरण असंभव है, इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार जरूरी है।
📅 समसामयिक प्रासंगिकता
आज भी जातिगत भेदभाव मौजूद है।
आरक्षण नीति सामाजिक न्याय के प्रयास का उदाहरण है।
तकनीकी युग में भी योग्यता आधारित चयन और व्यवसायिक स्वतंत्रता अत्यंत प्रासंगिक हैं।
🏁 निष्कर्ष
जाति प्रथा आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दृष्टि से हानिकारक है।
अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है।
पेशा चुनने की स्वतंत्रता और समान अवसर ही न्यायपूर्ण समाज की नींव हैं।
📜 सारांश
अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रमिक विभाजन बताते हुए उसकी कमियों और हानियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति की रुचि, योग्यता और स्वतंत्रता को खत्म कर देती है तथा बेरोजगारी को बढ़ाती है। उनके अनुसार आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर टिका हो। लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन नहीं बल्कि सामूहिक जीवन में समान सहभागिता और सम्मान है।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
पाठ्यपुस्तक के प्रश्न
❓ प्रश्न 1: जाति प्रथा को श्रम-विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आंबेडकर के क्या तर्क हैं?
💡 उत्तर: जाति प्रथा को श्रम-विभाजन का ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं –
⚠️ श्रमिक-विभाजन की समस्या – यह केवल कार्य का बंटवारा नहीं, बल्कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है।
⬆️⬇️ ऊंच-नीच का भाव – विभाजित वर्गों को श्रेष्ठ और हीन ठहराना, जो किसी अन्य समाज में नहीं है।
🎯 रुचि का अभाव – पेशा मनुष्य की रुचि और योग्यता पर नहीं, जन्म पर तय होता है।
📜 पूर्व-निर्धारण – माता-पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर जन्म से पहले ही पेशा तय।
🚫 लचीलेपन का अभाव – व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं, चाहे भूखों मरना पड़े।
❓ प्रश्न 2: जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है?
💡 उत्तर:
🔹 बेरोजगारी के कारण
🔒 पेशे में बंधन – जीवनभर एक ही पेशा अपनाने की बाध्यता।
⚙️ तकनीकी परिवर्तन – नई तकनीक आने पर भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं।
🏠 पैतृक पेशे की बाध्यता – जन्म से तय पेशा बदलना असंभव।
🔹 आधुनिक स्थिति
📚 शिक्षा, ⚖️ कानून और 🛠️ तकनीकी विकास ने जातिगत पेशा-बाध्यता को कमजोर किया है।
आज व्यवसाय बदलने में जाति बड़ी बाधा नहीं रही।
❓ प्रश्न 3: लेखक के मत से ‘दासता’ की व्यापक परिभाषा क्या है?
💡 उत्तर:
❌ केवल कानूनी पराधीनता नहीं – अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता छीनना भी दासता है।
🚫 व्यावसायिक स्वतंत्रता का हनन – पेशा चुनने के अधिकार का अभाव।
📏 निर्धारित आचरण की बाध्यता – दूसरों द्वारा तय किए नियमों को मानने के लिए विवश होना।
💭 मनोनुकूल आचरण का अभाव – अपनी इच्छा से कार्य न कर पाना।
❓ प्रश्न 4: शारीरिक वंश-परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से असमानता होने पर भी अंबेडकर ‘समता’ को क्यों व्यवहार्य मानते हैं?
💡 उत्तर:
🎯 समान अवसर – क्षमता विकास के लिए आवश्यक।
🛡️ भेदभाव का विरोध – जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर असमानता अनुचित।
📈 अधिकतम उपयोगिता – समान अवसर से समाज को अधिकतम लाभ मिलता है।
🏛️ राजनीतिक व्यावहारिकता – सभी को समान व्यवहार देना आसान और न्यायसंगत है।
🌱 सामाजिक उत्थान – स्वतंत्रता व समानता से ही समता संभव।
❓ प्रश्न 5: क्या आप सहमत हैं कि भावनात्मक समत्व के लिए भौतिक स्थितियां व जीवन-सुविधाएं समान होनी चाहिए?
💡 उत्तर: हाँ, पूर्ण सहमति है –
💞 भावनात्मक समत्व तभी संभव जब सभी को समान अवसर और सुविधाएं मिलें।
⚖️ समता जातिवाद के उन्मूलन की शर्त है।
💪 प्रयासों का सही मूल्यांकन समान अवसर पर ही संभव है।
🏫 सुविधाओं के अंतर से प्रतियोगिता का परिणाम प्रभावित होता है।
❓ प्रश्न 6: ‘भ्रातृता’ शब्द में क्या स्त्रियां भी सम्मिलित हैं?
💡 उत्तर: हाँ, यह शब्द लिंग-निरपेक्ष है –
🌏 भ्रातृता = विश्व बंधुत्व की भावना।
🙋♀️ स्त्रियां भी स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हैं।
🤝 यह सभी मनुष्यों को समान रूप से जोड़ता है।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
🔹 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
1️⃣ अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
(क) यह केवल श्रम विभाजन करती है
(ख) यह श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन भी करती है
(ग) यह केवल धर्म पर आधारित है
(घ) यह केवल आर्थिक असमानता लाती है
उत्तर: (ख)
2️⃣ अंबेडकर के आदर्श समाज के तीन स्तंभ कौन से हैं?
(क) धर्म, अर्थ, काम
(ख) सत्य, अहिंसा, करुणा
(ग) स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व
(घ) न्याय, शांति, प्रगति
उत्तर: (ग)
3️⃣ जाति प्रथा के कारण किसी व्यक्ति का व्यवसाय कब निर्धारित हो जाता है?
(क) जन्म के समय
(ख) गर्भधारण के समय
(ग) शिक्षा पूरी करने के बाद
(घ) विवाह के समय
उत्तर: (ख)
4️⃣ अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र क्या है?
(क) केवल शासन की एक पद्धति
(ख) केवल चुनाव प्रक्रिया
(ग) सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति
(घ) केवल राजनीतिक व्यवस्था
उत्तर: (ग)
5️⃣ मनुष्य की शक्ति किन तीन चीजों पर निर्भर करती है?
(क) धन, शिक्षा, जाति
(ख) शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, व्यक्तिगत प्रयत्न
(ग) बुद्धि, बल, धन
(घ) परिवार, समाज, राज्य
उत्तर: (ख)
🔹 लघु उत्तरीय प्रश्न
1️⃣ अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को ‘स्वाभाविक विभाजन’ क्यों नहीं माना है?
उत्तर. जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें पेशा जन्म से पहले ही तय कर दिया जाता है, जबकि स्वाभाविक विभाजन में व्यक्ति अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार पेशा चुनता है।
2️⃣ आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा कैसे समस्या बनती है?
उत्तर. तकनीकी बदलाव के समय पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, पर जाति प्रथा व्यक्ति को जीवनभर एक ही पेशे में बांध देती है, जिससे विकास रुकता है।
3️⃣ ‘दासता’ की अंबेडकर की परिभाषा पारंपरिक परिभाषा से कैसे अलग है?
उत्तर. पारंपरिक दासता कानूनी पराधीनता है, जबकि अंबेडकर के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होना भी दासता है।
4️⃣ ‘समता’ को नियंत्रक सिद्धांत क्यों बताया गया है?
उत्तर. राजनीतिक रूप से सभी को समान अवसर देना जरूरी है क्योंकि व्यावहारिक रूप से अलग-अलग मूल्यांकन संभव नहीं।
5️⃣ आदर्श समाज में ‘गतिशीलता’ क्यों आवश्यक है?
उत्तर. ताकि परिवर्तन और सुधार समाज में हर जगह समान रूप से फैल सकें और प्रगति संभव हो।
🔹 मध्यम उत्तरीय प्रश्न
1️⃣ जाति प्रथा से होने वाली आर्थिक हानियां
उत्तर. बेरोजगारी – पैतृक पेशे में बंधन
कुशलता का अभाव – अरुचि से कार्य
तकनीकी विकास में बाधा
मानव संसाधन और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग
2️⃣ अंबेडकर के आदर्श समाज की विशेषताएं
उत्तर. तीन स्तंभ – स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व
गतिशीलता – परिवर्तन का तेज संचार
सामूहिक भागीदारी – सबकी जिम्मेदारी
सामाजिक संपर्क के साधन
लोकतांत्रिक मूल्य और भाईचारा
3️⃣ स्वतंत्रता का सिद्धांत और जाति प्रथा का विरोध
उत्तर. आवागमन, संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता
व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता सर्वोपरि
जाति प्रथा इन स्वतंत्रताओं को खत्म करती है
स्वतंत्रता के बिना व्यक्तित्व विकास असंभव
4️⃣ अंबेडकर की ‘समता’ की अवधारणा
उत्तर. समान अवसर से अधिकतम उपयोगिता
राजनीतिक व्यावहारिकता में समान व्यवहार
सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक
कठिनाइयों के बावजूद नियंत्रक सिद्धांत
🔹 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
1️⃣.जाति प्रथा की आलोचना और आदर्श समाज की व्यावहारिकता
उत्तर. अंबेडकर ने जाति प्रथा को केवल श्रम विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिक विभाजन बताया। इसमें ऊंच-नीच का भाव, पूर्व-निर्धारित पेशा और पेशा बदलने की मनाही समाज और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इससे बेरोजगारी, कुशलता का अभाव और तकनीकी विकास में बाधा आती है।
उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है। इसमें व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, समान अवसर, भाईचारा और लोकतांत्रिक जीवनचर्या की परंपरा है। आज के भारत में संविधान, आरक्षण नीति और सामाजिक सुधार इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव अब भी मौजूद है। अंबेडकर का संदेश है कि वास्तविक प्रगति तभी होगी जब हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अवसर पा सके और समाज में समान सम्मान मिले।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
