Class 12 : हिंदी साहित्य – अध्याय 6.तुलसीदास
संक्षिप्त लेखक परिचय
🌟 जीवन:-
🔶 लोकमान्यता के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र के राजापुर में हुआ और उनका अधिकांश समय काशी में बीता।
🔷 आरंभिक जीवन में विपत्तियाँ झेलते हुए भी उन्होंने वैष्णव भक्ति परंपरा में दीक्षा लेकर रामभक्ति को जीवनाधार बनाया।
🔶 काशी में साधना, प्रवचन और रचना-कार्य के साथ उन्होंने लोकहित और नैतिकता को अपनी साधना का केंद्र रखा।
🔷 परंपरा मानती है कि उनका देहावसान काशी में हुआ; संपूर्ण जीवन में उन्होंने भक्ति, मर्यादा और करुणा का संदेश दिया।
🌟 साहित्यिक योगदान:-
💠 तुलसीदास ने भक्तिकाल को जनभाषा में नई ऊँचाई दी—अवधी और ब्रज में लिखकर उन्होंने वेदांत-विचार को सरल, भावपूर्ण और लोकोन्मुख बनाया।
💠 उनकी प्रमुख कृतियों में रामचरितमानस, विनयपत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली और परंपरागत रूप से उनसे संबद्ध हनुमान चालीसा अत्यंत लोकप्रिय हैं।
💠 रामचरितमानस ने मर्यादा, धर्म, सेवा, दया और प्रेम के आदर्शों को कथा-संगीत और लयात्मक छंदों—दोहा, चौपाई, सोरठा—में गूँथकर व्यापक समाज तक पहुँचाया।
💠 गीतावली और कवितावली में रसनिष्ठ भक्ति, प्रतीक-योजना, अनुप्रास और चित्रात्मकता के माध्यम से करुण, शांत और भक्ति रस का अद्भुत संपुट मिलता है; मातृ-प्रेम, भ्रातृ-प्रेम और दीन-जन के प्रति करुणा का कोमल विन्यास तुलसी-रचना का निजी हस्ताक्षर है।
💠 उनकी भाषा सरल संस्कारपूर्ण है—लोक-उदाहरण, नीति-वाक्य और भावगर्भित संवादों से वे पठनीयता और स्मरणीयता रचते हैं।
💠 हिन्दी साहित्य, कीर्तन-परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक मानस पर तुलसीदास का प्रभाव दूरगामी है; उनके आदर्श आज भी नैतिक शिक्षा, नागरिकता और मानवीय सह-अस्तित्व को दिशा देते हैं। ✨
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन
🌸 पंक्ति-दर-पंक्ति व्याख्या
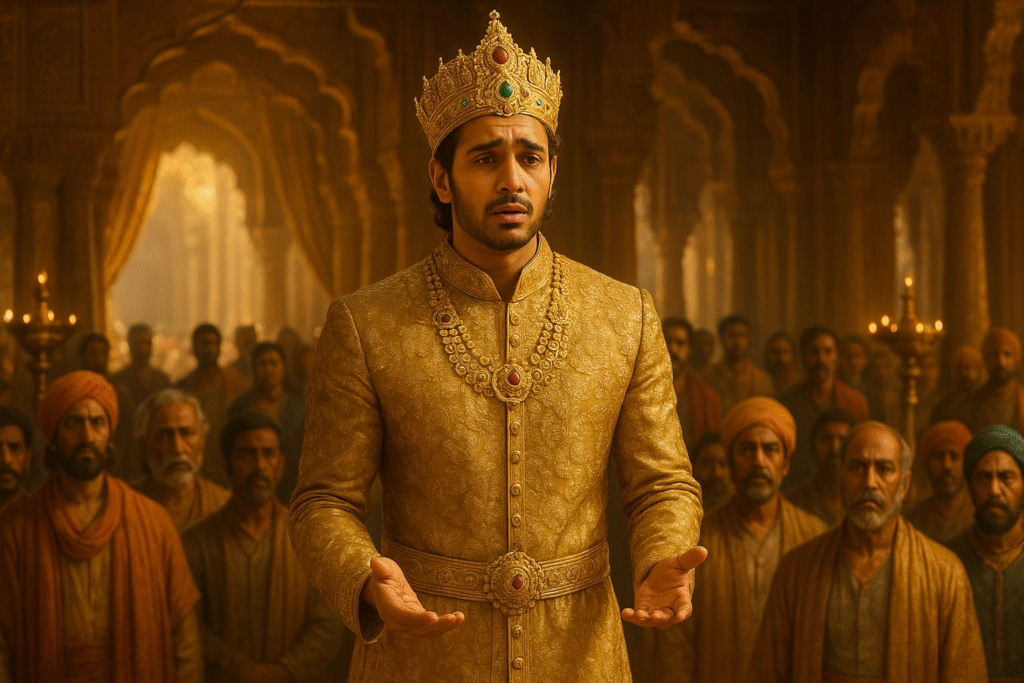
✨ भाग 1: भरत–राम का प्रेम (रामचरितमानस – अयोध्याकांड से)
🔹 “पुलकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े।।”
▫️ भरत को राम-दर्शन होते ही पूरे शरीर में रोमांच छा जाता है, कमल-जैसी आँखों में प्रेम के आँसू भर आते हैं।
🔹 “कहब मोर मुनिनाथ निभाहा। एहि तें अधिक कहौं मैं काहा।।”
▫️ गुरु वशिष्ठ ने सब कुछ कह दिया है, मैं उससे अधिक कुछ कह भी नहीं सकता—विनम्रता का भाव।
🔹 “मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ।।”
▫️ मैं अपने प्रभु राम का स्वभाव जानता हूँ—वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते।
🔹 “मो पर कृपा सनेह बिसेखी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी।।”
▫️ मेरे प्रति उनका स्नेह अद्वितीय है—खेलते समय भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया।
🔹 “सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहूँ न कीन्ह मोर मन भंगू।।”
▫️ बाल्यकाल से हमने साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा।
🔹 “मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही। हारेंहूँ खेल जितावहिं मोहीं।।”
▫️ प्रभु की कृपा-रीति यह है कि वे स्वयं हारकर भी मुझे जिता देते हैं।
🔹 “महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कहैं न बैन।।”
▫️ अत्यधिक स्नेह और संकोच के कारण मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ।
🔹 “दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैना।।”
▫️ दर्शन से मन तृप्त नहीं हुआ, आँखें प्रेम की प्यास से अभी भी भरी हैं।
🔹 “बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा।।”
▫️ विधाता मेरे और राम के प्रेम को सह न सके, माँ (कैकेयी) के बहाने दूरी डलवा दी।
🔹 “यहउ कहत मोहि आजु न सोभा। अपनी समुझि साधु सुचि को भा।।”
▫️ आज यह कहना भी उचित नहीं कि कौन साधु है और कौन नहीं।
🔹 “मातु मंदि मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली।।”
▫️ यदि मैं सोचूँ कि माँ नीच और मैं साधु—तो यह करोड़ों कुचालियों जैसा है।
🔹 “फरइ कि कोदव बालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक काली।।”
▫️ क्या कोदो की बाली उत्तम धान उपजा सकती है? क्या काली घोंघी मोती दे सकती है?
🔹 “सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाहू।।”
▫️ किसी पर दोष का लेश भी नहीं लगाना चाहता, मेरा अभाग्य ही अपार है।
🔹 “बिनु समुझें निज अघ परिपाकू। जारिउँ जायँ जननि कहि काकू।।”
▫️ अपने अपराध का परिणाम समझे बिना माँ को दोष देना अनुचित है।
🔹 “हृदय हेरि हरेउँ सब ओरा। एकहि भाँति भलेंहि भल मोरा।।”
▫️ हृदय में झाँका—सब ओर मेरा ही दोष है, राम का हित ही सर्वोपरि है।
🔹 “गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू।।”
▫️ गुरु, स्वामी, सीता-राम—सभी का निर्णय कल्याणकारी है।
🔹 “साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहहूँ सुथल सति भाउ।।”
▫️ साधु-सभा और प्रभु-सान्निध्य में भी मेरा भाव सच्चा और स्पष्ट है।
🔹 “प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ।।”
▫️ यदि मेरे प्रेम में झूठ होता, तो मुनि और रघुराज तुरंत जान लेते।
🔹 “भूपति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगु सबु साखी।।”
▫️ राजा दशरथ ने प्रेम-प्रतिज्ञा निभाकर प्राण त्याग दिए; माँ की कुमति जगजाहिर है।
🔹 “देखि न जाहिं बिकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं।।”
▫️ माताएँ विलाप करती हैं, नगर के नर-नारी वियोग से दहक रहे हैं।
🔹 “महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुझि सहिउँ सब सूला।।”
▫️ धरती के सभी अनर्थों की जड़ मैं हूँ—इसलिए सब कष्ट सहने को तैयार हूँ।
🔹 “सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि बेष लखन सिय साथा।।”
▫️ रघुनाथ लक्ष्मण और सीता संग मुनि-वेष में वन को चले गए।
🔹 “बिनु पानहिंह पयादेहि पाएँ। संकरु साखि रहेउँ ऐहि घाएँ।।”
▫️ वे नंगे पाँव कठिन मार्ग पर चले; शिव साक्षी हैं।
🔹 “बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू।।”
▫️ निषादराज का प्रेम देखकर भी मेरा वज्र-कठोर हृदय पिघला नहीं।
🔹 “अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड़ सबइ सहाई।।”
▫️ अब सब अपनी आँखों से देख लिया, जीवित प्राणी को जड़-सा कष्ट सहना पड़ता है।
🔹 “जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी। तजहिं बिषम बिषु तापस तीछी।।”
▫️ जिन्हें देखकर सर्प-बिच्छू भी विष छोड़ दें—ऐसे करुणामय राम।
🔹 “तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागो जाहि।।”
▫️ वही रघुनंदन, लक्ष्मण, सीता—कभी किसी का अनहित न करने वाले—शत्रु मान लिए गए।
🔹 “तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि।।”
▫️ ऐसी माता का पुत्र (मैं) क्यों न यह असह्य दुख सहूँ।
🌼 भाग 2: पद – “जननी निरखति बान धनुहियाँ…”
🔹 “जननी निरखति बान धनुहियाँ।”
▫️ माँ कौशल्या राम के बाल-धनुष-बाण को निहारती हैं।
🔹 “बार बार उर नैनि लावति प्रभुजू की ललित पनहियाँ।।”
▫️ राम की नन्हीं जूतियों को बार-बार हृदय और आँखों से लगाती हैं।
🔹 “कबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सवारे।”
▫️ जैसे पहले प्रेमभरे वचनों से जगाने जाती थीं।
🔹 “उठहु तात! बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे।।”
▫️ “उठो पुत्र! छोटे भाई और सखा द्वार पर हैं।”
🔹 “कबहुँ कहति यों ‘बड़ी बार भइ’ जाहु भूप पहँ, भैया।”
▫️ “देर हो गई बेटा, अब राज-काज को जाओ।”
🔹 “बंधु बोलि जेंइय जो भावै गई निछावरि मैया”
▫️ बंधुओं को बुलाकर जो अच्छा लगे, वही करो—माँ का ममत्व।
🔹 “कबहुँ समुझि वनगमन राम को रहि चकि चित्रलिखी सी।”
▫️ वनगमन याद आते ही चित्रवत् जड़ हो जाती हैं।
🔹 “तुलसीदास वह समय कहे तें लागति प्रीति सिखी सी।।”
▫️ प्रेम उस समय मोरनी जैसा लगता है—आनंद से वियोग तक।
🌺 भाग 3: पद – “राघौ! एक बार फिरि आवौ…”
🔹 “राघौ! एक बार फिरि आवौ।”
▫️ “हे राघव! एक बार लौट आओ।”
🔹 “ए बर बाजि बिलोकि आपने बहुरो बनहिं सिधावौ।।”
▫️ “इन घोड़ों को देख लो, फिर चाहो तो वन को लौट जाना।”
🔹 “जे पय प्याइ पोखि कर–पंकज वार वार चुचुकारे।”
▫️ जिन्हें तुमने हाथों से दुलारा, वे घोड़े भी उदास हैं।
🔹 “क्यों जीवहिं, मेरे राम लाडिले! ते अब निपट बिसारे।।”
▫️ “लाडिले राम! जिन्हें छोड़ दिया, वे कैसे जीवित रहें?”
🔹 “भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे।”
▫️ भरत पूरी लगन से उनकी सेवा कर रहे हैं।
🔹 “तदपि दिनहिं दिन होत झाँवरे मनहुँ कमल हिममारे।।”
▫️ फिर भी वे मुरझा रहे हैं—जैसे हिम से पीड़ित कमल।
🔹 “सुनहु पथिक! जो राम मिलहिं बन कहियौ मातु संदेसो।”
▫️ “हे पथिक! यदि राम मिलें तो माँ का संदेश कहना।”
🔹 “तुलसी मोहिं और सबहिन तें इन्हको बड़ो अंदेसो।।”
▫️ “मुझे सबसे अधिक इन घोड़ों की चिंता है।”
🌟 गहन भाव-सार
🌿 पहला अंश – भरत–राम का प्रेम
गोस्वामी तुलसीदास का यह अंश भाईचारे, त्याग, और धर्म-पालन के उच्चतम आदर्श का अमर उदाहरण है। कथा का प्रसंग राम के वनवास काल से जुड़ा है, जब भरत, राम को अयोध्या लौटाने का आग्रह लेकर चित्रकूट आते हैं। पिता दशरथ का निधन हो चुका है, राज्य खाली है, और समस्त अयोध्यावासी राम को अपना राजा बनाना चाहते हैं।
अंश की शुरुआत में भरत का भावनात्मक रूप सामने आता है — राम के दर्शन मात्र से उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, आँखों में आँसू भर आते हैं, और वाणी गले में अटक जाती है। यहाँ तुलसीदास ने प्रेम के अवरोधक पक्ष को दिखाया है — अत्यधिक स्नेह और सम्मान वाणी को रोक देता है।
भरत राम के स्वभाव की प्रशंसा करते हैं — कहते हैं कि राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, उनके स्नेह में कभी कमी नहीं आई। बचपन से अब तक राम ने उन्हें कभी आहत नहीं किया। यहाँ भरत का दृष्टिकोण पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों से प्रमाण देते हैं कि राम का व्यवहार सदा उदार, स्नेहमय और सौम्य रहा है।
भरत अपनी माँ कैकेयी के षड्यंत्र का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे माँ को पूरी तरह दोष नहीं देते। इसके बजाय वे स्वयं को दोषी मानते हैं — कहते हैं कि यदि मैं उत्तम हूँ तो माता भी दोषरहित मानी जाएगी; यदि संतान में दोष है तो यह माता के संस्कारों का परिणाम है। यहाँ आत्मनिंदा और विनम्रता का अद्भुत संगम है। वे उपमा देकर कहते हैं — क्या कोदो की बाली उत्तम धान उत्पन्न कर सकती है, या काली घोंघी मोती दे सकती है? यह उनका स्वयं को दोषी ठहराने का तरीका है, ताकि वे किसी और पर आरोप न लगाएँ।
भरत बार-बार दोहराते हैं कि वे किसी पर दोषारोपण का विचार भी नहीं लाना चाहते। उनका मानना है कि उनका अभाग्य ही सभी कष्टों का कारण है। यही धर्म और मर्यादा का भाव है — अपनी पीड़ा को सहते हुए भी दूसरों पर दोष न देना।
इसके बाद भरत राम के वन-गमन के दृश्य को स्मरण करते हैं — नंगे पाँव, कठोर मार्ग, सीता और लक्ष्मण के साथ राम का मुनि-वेष धारण कर प्रस्थान करना। वे निषादराज के स्नेह का वर्णन करते हैं और स्वयं पर अफसोस करते हैं कि उनका हृदय उस समय भी नहीं पिघला।
अंत में भरत कहते हैं — यदि मेरे प्रेम में छल या दिखावा होता, तो मुनि और राम तुरन्त समझ लेते। वे अपने प्रेम की सत्यता पर गर्व करते हैं, लेकिन यह गर्व भी विनम्रता से लिपटा हुआ है। वे मानते हैं कि राम का निर्णय ही अंतिम और कल्याणकारी है, चाहे वह उनके विरुद्ध क्यों न हो।
इस पूरे अंश में भाईचारे का आदर्श रूप उभरता है — एक ओर भरत का त्याग, जो स्वयं राजगद्दी स्वीकार नहीं करते और नन्दीग्राम में राम की चरणपादुका स्थापित कर राज्य संचालन करते हैं; दूसरी ओर राम का वचनपालन, जो पिता की आज्ञा और अपने धर्म के प्रति अडिग रहते हैं। तुलसीदास ने इस मिलन दृश्य में करुण रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है।
यह अंश हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार जताने में नहीं, बल्कि त्याग और निष्ठा में है। भरत का राम के प्रति प्रेम केवल पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पण भी है। यही कारण है कि भरत भारतीय संस्कृति में मर्यादा, निष्ठा और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं।
🌼 दूसरा पद – “जननी निरखति बान धनुहियाँ…”
इस पद में तुलसीदास ने माँ कौशल्या के हृदय की वात्सल्य-पीड़ा को अत्यंत मार्मिकता से चित्रित किया है। राम के वनवास के बाद माँ उनके स्मृति-चिह्नों में ही जीवन का सहारा खोजती है। वह राम के बचपन के खिलौने, धनुष-बाण, और नन्हीं पनहियाँ (जूते) को बार-बार निहारती और सीने से लगाती है।
पद की पंक्तियाँ माँ की स्मृतियों का जाल बुनती हैं — जैसे पहले वह राम को सुबह जगाने जाती थीं, प्रिय वचन बोलती थीं, राजकाज के लिए भेजती थीं, दोस्तों और भाइयों के साथ खेलने के लिए प्रेरित करती थीं। अब यह सब केवल स्मृति में ही संभव है।
वनगमन का प्रसंग याद आते ही माँ कौशल्या का हृदय स्तब्ध हो जाता है, मानो समय ठहर गया हो। तुलसीदास ने इसे “चित्रलिखी सी” उपमा से सजाया है — जैसे कोई चित्र दीवार पर स्थिर हो, वैसे ही माँ वियोग के क्षण में जड़ हो जाती है।
अंतिम पंक्ति में प्रेम को “सिखी” (मोरनी) की उपमा दी गई है। जैसे मोरनी आनंद में नाचती है, पर अपने पैरों को देख दुखी हो जाती है, वैसे ही माँ का प्रेम भी स्मृतियों में आनंदित होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर दुखी हो जाता है। यह वियोग और स्मृति का द्वंद्व है, जो पद की आत्मा है।
🌺 तीसरा पद – “राघौ! एक बार फिरि आवौ…”
यह पद भी माँ कौशल्या की करुण वाणी का विस्तार है, लेकिन इसमें एक नया बिंब आता है — घोड़ों का प्रसंग। माँ राम से कहती हैं कि “एक बार आकर इन घोड़ों को देख लो, फिर चाहो तो वन लौट जाना।”
ये वही घोड़े हैं, जिन्हें राम ने स्वयं जल पिलाया, दुलारा और अपने हाथों से सँवारा। अब ये घोड़े भी राम के वियोग में उदास और मुरझाए हुए हैं। माँ कहती हैं कि भरत उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि घोड़े राम के प्रिय हैं, लेकिन सेवा के बावजूद घोड़े दिन-प्रतिदिन मुरझा रहे हैं — जैसे हिम-पीड़ित कमल।
माँ की यह बात केवल घोड़ों के लिए चिंता नहीं है, बल्कि यह राम-वियोग के सार्वत्रिक प्रभाव का प्रतीक है — जैसे राजा का वियोग प्रजा, पशु-पक्षी, और सम्पूर्ण वातावरण पर असर डालता है।
अंत में माँ पथिक से कहती हैं — यदि वन में राम मिलें, तो मेरा यह संदेश पहुँचा देना। वह संदेश यह है कि मुझे सबसे अधिक चिंता इन घोड़ों की है। यह वाक्य माँ की ममता का अनूठा रूप दिखाता है — यहाँ पुत्र-प्रेम तो है ही, साथ ही उन जीवों के प्रति भी करुणा है जो पुत्र के स्नेह से जुड़े हैं।
यह पद करुण रस से ओतप्रोत है, और इसमें तुलसीदास ने वात्सल्य और करुणा का सुंदर संयोग रचा है।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
पाठ्यपुस्तक के प्रश्न
🌿 भरत-राम का प्रेम
❓ प्रश्न 1. ‘हारेंहु खेल जितावहिं मोही’ भरत के इस कथन का क्या आशय है?
✅ उत्तर: इस कथन के माध्यम से भरत श्रीराम के अनन्य स्नेह और बड़प्पन की भावना को प्रकट करते हैं।
🌟 भरत कहते हैं कि श्रीराम में बचपन से ही महान व्यक्तित्व के गुण थे।
💖 वे अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे और कभी भी उनका मन नहीं दुखाते थे।
🎯 खेल खेलते समय जब भी भरत हारने लगते थे, तो राम जानबूझकर स्वयं हार जाते थे और भरत को जिता देते थे।
😊 यह कार्य राम इसलिए करते थे ताकि भरत के मन को कोई चोट न पहुंचे और उनका उत्साह बना रहे।
🌺 राम सदा अपने से छोटों का उत्साहवर्धन करते रहे हैं और अपने बड़े होने का लाभ नहीं उठाते थे।
🌿 वे अपने छोटे भाइयों का बहुत ध्यान रखते थे और उन्हें प्रसन्न देखने के लिए स्वयं जान-बूझकर हार जाते थे।
🌼 इस प्रकार यह कथन राम की दयालुता, भातृप्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जहाँ वे अपने छोटे भाई की खुशी को अपनी विजय से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे।
❓ प्रश्न 2. ‘मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ’ में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है?
✅ उत्तर: इस कथन के माध्यम से भरत राम के स्वभाव की अनेक उत्कृष्ट विशेषताओं का उल्लेख करते हैं –
💖 दयालुता और क्षमाशीलता: राम का स्वभाव ऐसा है कि वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। वे सभी के प्रति प्रेम, दया, ममता और करुणा रखते हैं।
🌺 छोटों के प्रति विशेष स्नेह: भरत कहते हैं कि राम के मन में अपने छोटे भाइयों के प्रति विशेष प्रेम और स्नेह है। वे कभी किसी के मन को नहीं दुखाते।
🌿 धैर्य और सहनशीलता: राम खेल में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते थे परंतु दूसरों को कष्ट नहीं देते थे।
🌼 त्याग और निःस्वार्थता: राम अपनी इच्छाओं का त्याग करके दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं। वे स्वयं हारकर अपने भाइयों को जिता देते हैं।
❓ प्रश्न 3. भरत का आत्म-परिताप उनके चरित्र के किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है?
✅ उत्तर: भरत का आत्म-परिताप उनके चरित्र के अनेक उज्ज्वल पक्षों को दर्शाता है –
🌟 सत्यनिष्ठा और निर्दोषता: भरत का परिताप यह सिद्ध करता है कि वे सच्चे और निष्कपट हैं। राम को वनवास दिलाने में उनका कोई हाथ नहीं था।
💖 भ्रातृप्रेम की गहराई: जैसे ही उन्हें राम के वनवास का पता चला, वे तुरंत उन्हें लौटा लाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए।
🌿 आत्म-ग्लानि और विनम्रता: वे स्वयं को अभागा मानते हैं और राम को अपना स्वामी, स्वयं को सेवक कहते हैं।
🌼 नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता: उन्हें राज्य का कोई लालच नहीं है और वे किसी राजनीतिक षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहते।
❓ प्रश्न 4. राम के प्रति अपने श्रद्धाभाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं?
✅ उत्तर: भरत अनेक प्रकार से अपने श्रद्धाभाव को व्यक्त करते हैं –
🌟 शारीरिक अभिव्यक्ति: चित्रकूट की सभा में राम के सामने उनका शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते हैं।
💬 मौखिक स्वीकारोक्ति: वे राम को ‘स्वामी’ कहकर संबोधित करते हैं और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं।
🌺 राम के गुणों का गुणगान: वे राम की दयालुता, क्षमाशीलता और स्नेह का उल्लेख करते हैं।
🌿 निरंतर दर्शन की लालसा: वे कहते हैं कि उनके नेत्र कभी भी राम के दर्शन से तृप्त नहीं होते।
🌼 आत्म-समर्पण: वे प्रेम और संकोच के कारण राम के सामने मुख नहीं खोलते, जो उनके पूर्ण समर्पण को दर्शाता है।
❓ प्रश्न 5. ‘महीं सकल अनरथ कर मूला’ पंक्ति द्वारा भरत के विचारों-भावों का स्पष्टीकरण कीजिए।
✅ उत्तर: इस पंक्ति में भरत की आत्म-दोष भावना और गहरी पीड़ा झलकती है –
🌟 आत्म-दोष की भावना: वे स्वयं को धरती पर सभी अनर्थों का कारण मानते हैं।
💔 व्यापक कष्ट की अनुभूति: अयोध्यावासी और माताएँ राम-वियोग में दुख से व्याकुल हैं।
🌿 राम के कष्ट की स्मृति: वे राम के नंगे पाँव वन गमन का दृश्य याद करते हैं।
🌼 जीवित रहने का दुख: वे आश्चर्य करते हैं कि इतने दुख के बाद भी वे जीवित कैसे हैं।
🙏 प्रायश्चित की भावना: वे अपने पापों और माँ को कहे कटु वचनों के लिए पछतावा करते हैं।
🌸 पद
❓ प्रश्न 1. राम के वन-गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं?
✅ उत्तर:
🌟 स्मृतिजन्य वेदना: छोटे-छोटे धनुष और बाण देखकर सुखद क्षण याद करती हैं, जो अब पीड़ा का कारण हैं।
💖 भावनात्मक लगाव: राम की जूतियों को बार-बार आँखों और सीने से लगाती हैं।
🌿 भ्रम की स्थिति: कभी राम को जगाने का अभिनय करती हैं।
🌼 दैनिक जीवन का अनुकरण: जैसे अतीत में उनसे कहती थीं, वैसे ही बात करती हैं।
💔 चेतना की वापसी: वनगमन की याद आते ही चित्रवत् स्थिर हो जाती हैं।
❓ प्रश्न 2. ‘रहि चकि चित्रलिखी-सी’ पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।
✅ उत्तर:
🌟 अचेतन अवस्था: वनगमन की वास्तविकता याद आते ही कौशल्या स्तब्ध हो जाती हैं।
💔 शोक की तीव्रता: वे भौतिक संसार से कटकर चित्रवत् हो जाती हैं।
🌿 मनोवैज्ञानिक वास्तविकता: अत्यधिक शोक में चेतना लुप्त हो जाती है।
🌼 काव्य सौंदर्य: उपमा द्वारा उनकी पीड़ा का सजीव चित्रण हुआ है।
❓ प्रश्न 3. गीतावली से संकलित पद ‘राघौ एक बार फिरि आवौ’ में निहित करुणा और संदेश को स्पष्ट कीजिए।
✅ उत्तर:
💖 मातृ-प्रेम की करुणा: कौशल्या राम से एक बार लौट आने का निवेदन करती हैं।
🐎 जीवों के प्रति करुणा: वे राम के प्रिय घोड़ों की दुर्दशा का वर्णन करती हैं।
🌿 समर्पित सेवा का संदेश: भरत उनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि वे राम को प्रिय हैं।
💔 वियोग की पीड़ा: घोड़े दिन-प्रतिदिन मुरझा रहे हैं।
🌼 सार्वभौमिक संदेश: सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है।
❓ प्रश्न 4. (क) उपमा अलंकार के दो उदाहरण छाँटिए।
✅ उत्तर:
🌟 “रहि चकि चित्रलिखी-सी” – कौशल्या की स्थिर अवस्था की तुलना चित्र से।
🌸 “लागति प्रीति सिखी-सी” – प्रेम की तुलना मोरनी से।
(ख) उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है?
🌟 “मनहुँ कमल हिममारे” में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
💡 यहाँ घोड़ों की दशा को हिम से मुरझाए कमलों से तुलना कर भाव को मार्मिक बनाया गया है।
❓ प्रश्न 5. पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था।
✅ उत्तर:
🌟 द्विभाषिक प्रवाहता: अवधी व ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार।
✨ अलंकारों का कुशल प्रयोग:
अनुप्रास: “नीरज नयन नेह जल बाढ़े”
रूपक: “नीरज-नयन”, “कर-पंकज”
उपमा: “चित्रलिखी-सी”, “सिखी-सी”
उत्प्रेक्षा: “मनहुँ कमल हिममारे”
🎶 छंद विधान की निपुणता: दोहा-चौपाई और पद शैली में लयबद्धता।
🌼 भावानुकूल शब्द चयन: भाव के अनुसार शब्दों का प्रयोग।
🌿 लोक भाषा का प्रयोग: जनसाधारण तक भाव पहुँचाने के लिए।
❓ प्रश्न 6. पाठ के किन्हीं चार स्थानों पर अनुप्रास के स्वाभाविक एवं सहज प्रयोग हुए हैं, उन्हें छाँटकर लिखिए।
✅ उत्तर:
🌟 “नीरज नयन नेह जल बाढ़े” – ‘न’ वर्ण की आवृत्ति।
🌸 “दुसह दुःख दैव सहावइ” – ‘द’ वर्ण की आवृत्ति।
🌿 “जारिउँ जायँ जननि कहि काकू” – ‘ज’ वर्ण की आवृत्ति।
🌼 “पुलकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े” – ‘स’ और ‘भ’ वर्ण की आवृत्ति।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
🎯 5 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
1 ‘रामचरितमानस’ के किस कांड से ‘भरत-राम का प्रेम’ का अंश लिया गया है?
(a) बालकांड
(b) अयोध्याकांड ✅
(c) अरण्यकांड
(d) लंकाकांड
2 गीतावली में प्रयुक्त भाषा कौन सी है?
(a) अवधी
(b) ब्रजभाषा ✅
(c) खड़ी बोली
(d) मैथिली
3 ‘पुलकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े’ में कौन सा अलंकार है?
(a) उपमा
(b) रूपक
(c) अनुप्रास ✅
(d) उत्प्रेक्षा
4 भरत के अनुसार राम का मुख्य स्वभाव क्या है?
(a) क्रोधी होना
(b) अपराधी पर भी क्रोध न करना ✅
(c) कठोर व्यवहार
(d) उदासीन रहना
5 गीतावली के पदों में माता कौशल्या किससे राम को वापस आने की विनती करती है?
(a) धनुष-बाण के कारण
(b) प्रजा के कारण
(c) घोड़ों के कारण ✅
(d) महल के कारण
✏ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न (15 शब्द)
1 भरत राम को किस संबोधन से पुकारते हैं और क्यों?
उत्तर:
✅ भरत राम को ‘स्वामी’ कहते हैं क्योंकि वे राम को अपना स्वामी मानकर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं।
2 गीतावली की काव्य शैली की मुख्य विशेषता क्या है?
उत्तर:
✅ गीतावली प्रगीतात्मक शैली में रचित है जिसमें राम-कथा के मार्मिक प्रसंग गीत रूप में हैं।
3 भरत अपने आत्म-दोष की भावना कैसे व्यक्त करते हैं?
उत्तर:
✅ भरत कहते हैं “महीं सकल अनरथ कर मूला” यानी वे स्वयं को सभी अनर्थों का मूल मानते हैं।
4 माता कौशल्या की दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया है?
उत्तर:
✅ वे सुबह राम के कमरे में जाकर उन्हें जगाने का अभिनय करती हैं और भ्रम में रहती हैं।
5 ‘नीरज नयन’ में कौन सा अलंकार और अर्थ निहित है?
उत्तर:
✅ इसमें रूपक अलंकार है, जिसका अर्थ है – कमल के समान सुंदर नेत्र।
📜 4 मध्यम उत्तरीय प्रश्न (70 शब्द)
1 तुलसीदास ने गीतावली की रचना क्यों की और इसकी क्या विशेषताएं हैं?
उत्तर:
✅ तुलसीदास ने गीतावली की रचना सूरदास के प्रभाव से कृष्ण काव्य परंपरा की गीत पद्धति पर राम कथा प्रस्तुत करने के लिए की। इसमें राम के चरित की मार्मिक घटनाएं, झांकियां और करुण दशाओं को प्रगीतात्मक शैली में पिरोया गया है। यह ब्रजभाषा में रचित है और इसमें 328 पद हैं जो सात कांडों में विभाजित हैं।
2 चित्रकूट की सभा में भरत की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
✅ सभा में भरत का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले। वे भावुक होकर रो पड़े और विनम्रता से कहा कि गुरु वशिष्ठ ने सब कह दिया है। यह दशा उनके गहरे प्रेम और श्रद्धा को दर्शाती है।
3 माता कौशल्या के वियोग की पीड़ा का मनोवैज्ञानिक चित्रण कैसे किया गया है?
उत्तर:
✅ कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर कभी आंखों से लगाती हैं तो कभी हृदय से। भ्रम में राम को जगाने का अभिनय करती हैं। वास्तविकता का बोध होते ही ‘चित्रलिखी-सी’ स्तब्ध हो जाती हैं।
4 गीतावली में तुलसीदास की काव्य-कला की क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं?
उत्तर:
✅ इसमें संस्कृत तत्सम शब्दावली का प्रयोग, हृदय के भावों की मधुर पदों में व्यंजना, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, गेयता और संगीतात्मकता विद्यमान है।
📖 1 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (150 शब्द)
1 ‘भरत-राम का प्रेम’ और ‘पद’ के आधार पर तुलसीदास की भाषा-शैली और अलंकार योजना की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:
✅ तुलसीदास की भाषा-शैली परिष्कृत और प्रभावशाली है। ‘भरत-राम का प्रेम’ में अवधी, जबकि ‘पद’ में ब्रजभाषा का प्रवाह है।
अलंकार योजना में अनुप्रास का प्रयोग – “नीरज नयन नेह जल”, “दुसह दुःख दैव” में वर्ण की आवृत्ति से संगीतात्मकता आती है।
रूपक – “नीरज नयन”, “कर-पंकज” सुंदर हैं।
उपमा – “चित्रलिखी-सी”, “सिखी-सी” प्रभावशाली हैं।
उत्प्रेक्षा – “मनहुं कमल हिममारे” मार्मिक है।
छंद विधान में दोहा-चौपाई और गीतावली में पद शैली का प्रयोग है।
भावानुकूल शब्द-चयन, लोकभाषा का प्रयोग, करुणा और प्रेम के भावों की सजीव अभिव्यक्ति इनकी भाषा-शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
