Class 12 : हिंदी अनिवार्य – अध्याय 3 कविता के बहाने, बात सीधी थी पर
संक्षिप्त लेखक परिचय
कुंवर नारायण का जन्म 19 सितम्बर 1927 को फ़ैज़ाबाद (अब अयोध्या), उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख आधुनिक कवि, आलोचक और चिंतक थे। उनकी कविताओं में इतिहास-बोध, दर्शन, मानवता और आधुनिक जीवन की जटिलताओं का गहरा चित्रण मिलता है। उन्होंने कविता के साथ-साथ आलोचना, कहानी और निबंध लेखन में भी विशेष स्थान बनाया। उनकी रचनाएँ विचारशीलता और संवेदनशीलता से भरपूर होती हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए।
प्रमुख रचनाएँ (कविता संग्रह):
1️⃣ चक्रव्यूह
2️⃣ आत्मजयी
3️⃣ कोई दूसरा नहीं
4️⃣ वाजश्रवा के बहाने
उनका निधन 15 नवम्बर 2017 को हुआ। वे हिंदी साहित्य के गंभीर विचारधारा-प्रधान रचनाकार रहे।
—————————————————————————————————————————————————————
पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन
🔷 प्राकृतिक तत्वों से कविता की तुलना
कुँवर नारायण जी की “कविता के बहाने” एक गहन दार्शनिक कविता है जो कविता की असीमित शक्ति और महत्व को चिड़िया, फूल और बच्चों के माध्यम से समझाती है।
🐦 कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है, लेकिन कहा गया है कि
➡️ कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक व्यापक है।
🐦 चिड़िया की उड़ान भौतिक सीमाओं में बंधी है,
🎨 जबकि कविता कल्पना के पंखों से काल और स्थान की हर सीमा को पार कर जाती है।
🟢
🔷 फूल से कविता की श्रेष्ठता
🌸 फूल की तुलना में कवि बताते हैं कि जहाँ फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, वहीं
➡️ कविता “बिना मुरझाए महकने” की क्षमता रखती है।
🌺 कविता का सौंदर्य और सुगंध कालजयी होता है।
🕰️ यह समय के साथ नष्ट नहीं होती बल्कि युगों तक मानवता को प्रभावित करती रहती है।
🟢
🔷 बच्चों के खेल जैसी निर्बाध गति
👦👧 सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बच्चों के खेल का है।
जिस प्रकार बच्चे खेलते समय
➡️ “सब घर एक कर देने” की भावना से भेदभाव भूलकर हर जगह निर्बाध रूप से खेलते हैं,
उसी प्रकार कविता भी सभी बंधनों को तोड़कर मानवीय एकता का संदेश देती है।
🎈 कविता में भी वही निर्दोषता, सरलता और सार्वभौमिकता होती है जो बच्चों के खेल में होती है।
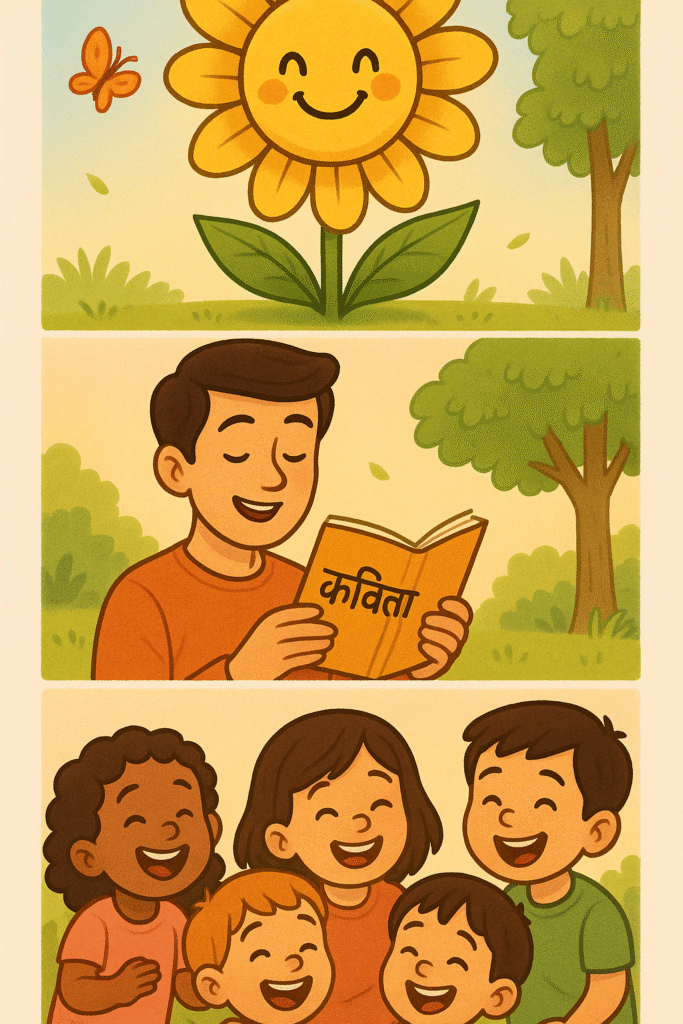
🟢
🔷 कविता का दार्शनिक महत्व
📜 कुँवर नारायण इस कविता में कविता के अस्तित्व पर आधुनिक युग की चुनौतियों के बीच प्रश्न उठाते हैं।
वे दिखाते हैं कि कविता केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को जीवित रखने का माध्यम है।
✨ यह कविता अंततः कविता की अमरता और उसकी सृजनात्मक शक्ति का उत्सव मनाती है।
🌟 कुंवर नारायण – कविता “बात सीधी थी” |
🔶
कविता की शुरुआत एक सीधी लेकिन प्रभावशाली पंक्ति से होती है – “बात सीधी थी पर वह भटक गया।” यह पंक्ति दर्शाती है कि जब व्यक्ति अपनी सरल बात को अनावश्यक तर्कों, द्वंद्वों और भ्रमों में उलझा देता है, तब वह बात अपने मूल अर्थ से दूर हो जाती है।
🌈
कवि यहाँ यह इंगित करते हैं कि मनुष्य अपनी सोच को इतना उलझा देता है कि जो बात साफ-साफ कही जा सकती थी, वह भी अस्पष्ट लगने लगती है। यह मानसिक जटिलता जीवन के अनुभवों, विचारों और व्याख्याओं के कारण उत्पन्न होती है, जिससे सत्य ओझल हो जाता है।
💠
कविता में समाज की उस प्रवृत्ति की आलोचना है जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग साधारण बातों को भी तर्क, दर्शन और विचारधाराओं में उलझा देता है। कुंवर नारायण इस भटकाव को दर्शाते हैं कि कैसे ‘सीधी बात’ भी अर्थहीन हो जाती है जब उस पर अनावश्यक आवरण चढ़ा दिया जाता है।
🌟
अंततः कवि एक सशक्त संदेश देते हैं कि सत्य और सरलता को जटिलता में न उलझाया जाए। अगर हम सहज और स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, तो हर बात का मूल भाव समझा जा सकता है। कविता हमें आत्ममंथन करने को प्रेरित करती है – क्या हम भी बातों को अनावश्यक रूप से कठिन तो नहीं बना रहे?
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
पाठ्यपुस्तक के प्रश्न
🔷 प्रश्न 1:
इस कविता के बहाने बताएं कि ‘सब घर एक करे देने के मानें’ क्या है?
🔶 उत्तर:
‘सब घर एक करे देने के मानें’ का आशय यह है कि कविता में ऐसी शक्ति होती है जो विभिन्न घरों, परिवारों और हृदयों को एकजुट कर देती है। कविता सभी को एक साथ बांधने की क्षमता रखती है – चाहे वे अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्कृति या विचारधारा से आते हों।
🌸 कविता की भावनात्मक अपील और सार्वभौमिक संदेश सभी मनुष्यों के हृदय को छूकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है।
🔷 प्रश्न 2:
‘उड़ने’ और ‘बिखरने’ का कविता से क्या संबंध बनता है?
🔶 उत्तर:
कविता में ‘उड़ने’ और ‘बिखरने’ के दो मुख्य अर्थ हैं:
✳️ उड़ना: कविता की कल्पना और भावनाओं की उच्च उड़ान को दर्शाता है। कवि अपनी कल्पना के पंखों पर भावनाओं को ऊंचाइयों तक ले जाता है।
✳️ बिखरना: कविता का व्यापक प्रसार और प्रभाव दिखाता है। जैसे फूल की सुगंध चारों ओर बिखरती है, वैसे ही कविता के भाव और संदेश समाज में दूर-दूर तक फैलते हैं।
🔷 प्रश्न 3:
कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं?
🔶 उत्तर:
कविता और बच्चों में निम्नलिखित समानताएं हैं:
🌼 स्वाभाविकता और सरलता: दोनों में प्राकृतिक स्वाभाविकता होती है।
🌼 कल्पनाशीलता: बच्चों की तरह कविता भी कल्पना से भरपूर होती है।
🌼 निर्दोषता और शुद्धता: दोनों में कृत्रिमता नहीं होती।
🌼 सहजता: बच्चों की भांति कविता भी सहज रूप से मन को प्रभावित करती है।
🔷 प्रश्न 4:
कविता के संदर्भ में ‘बिना मुरझाए महकने के मानें’ क्या होते हैं?
🔶 उत्तर:
‘बिना मुरझाए महकने के मानें’ से तात्पर्य कविता की शाश्वत और अमर प्रकृति से है:
🌸 कालजयी गुणवत्ता: अच्छी कविता समय के साथ मुरझाती या पुरानी नहीं होती।
🌸 स्थायी प्रभाव: इसका प्रभाव और सुगंध लंबे समय तक बनी रहती है।
🌸 सदैव ताजा: कविता हमेशा नई और ताजी लगती है, बासी नहीं होती।
🔷 प्रश्न 5:
‘भाषा को सहूलियत’ से बरतने से क्या अभिप्राय है?
🔶 उत्तर:
‘भाषा को सहूलियत से बरतना’ का अर्थ है:
💠 सरल और स्वाभाविक प्रयोग: भाषा का कुशल और आसान उपयोग करना।
💠 प्रवाहमयता: भाषा में अड़चन न होना, स्वाभाविक बहाव होना।
💠 संप्रेषणीयता: भाव और विचारों को आसानी से पहुंचाना।
💠 कलात्मक प्रयोग: भाषा के साथ खेलना और उसे कलात्मक रूप देना।
🔷 प्रश्न 6:
बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में ‘सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है’ कैसे?
🔶 उत्तर:
भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी होने के कारण:
🔸 अनावश्यक अलंकरण: जब भाषा में अत्यधिक अलंकार और चमत्कार का प्रयोग होता है।
🔸 जटिल शब्दावली: कठिन और दुरुह शब्दों का अनुचित प्रयोग।
🔸 कृत्रिमता: स्वाभाविकता के स्थान पर कृत्रिम भाषा का प्रयोग।
🔸 व्याकरण की जटिलता: अत्यधिक व्याकरणिक नियमों में उलझना।
🔷 प्रश्न 7:
बात (कथ्य) के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित विवेक/मुहावरों से मिलान करें।
🔶 उत्तर:
🎀 सही मिलान:
🔹 बात की चूड़ी मर जाना ➔ बात में कसावट का न होना, बात का प्रभावहीन हो जाना।
🔹 बात की पेंच खोलना ➔ बात को सुलझाना, स्पष्ट करना।
🔹 बात का शरासर बच्चों की तरह खेलना ➔ बात का सरल और सहज होना।
🔹 पेंच को कील की तरह ठोंक देना ➔ बात को दृढ़ता से स्थापित करना।
🔹 बात का बन जाना ➔ कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
🔷 प्रश्न 1:
कुँवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ?
🔸 (क) 19 सितम्बर 1926, लखनऊ
🔸 (ख) 19 सितम्बर 1927, फैज़ाबाद
🔸 (ग) 20 सितम्बर 1928, दिल्ली
🔸 (घ) 18 सितम्बर 1925, इलाहाबाद
✅ उत्तर: (ख) 19 सितम्बर 1927, फैज़ाबाद
🔷 प्रश्न 2:
‘कविता के बहाने’ कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है?
🔸 (क) ‘चक्रव्यूह’ से
🔸 (ख) ‘परिवेश: हम-तुम’ से
🔸 (ग) ‘इन दिनों’ से
🔸 (घ) ‘कोई दूसरा नहीं’ से
✅ उत्तर: (ग) ‘इन दिनों’ से
🔷 प्रश्न 3:
कुँवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला?
🔸 (क) 2008 में
🔸 (ख) 2009 में
🔸 (ग) 2005 में (दिया 2009 में)
🔸 (घ) 2010 में
✅ उत्तर: (ग) 2005 में (दिया 2009 में)
🔷 प्रश्न 4:
‘बिना मुरझाए महकने के माने’ में कौन सा अलंकार है?
🔸 (क) उपमा अलंकार
🔸 (ख) अनुप्रास अलंकार
🔸 (ग) विरोधाभास अलंकार
🔸 (घ) उत्प्रेक्षा अलंकार
✅ उत्तर: (ग) विरोधाभास अलंकार
📌 व्याख्या: ‘बिना मुरझाए महकना’ में विरोधाभास है क्योंकि सामान्यतः महकने के लिए पहले मुरझाना आवश्यक होता है।
🔷 प्रश्न 5:
कवि के अनुसार कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
🔸 (क) वह सुंदर होती है
🔸 (ख) वह असीमित और कालजयी होती है
🔸 (ग) वह समझने में कठिन होती है
🔸 (घ) वह केवल कवियों के लिए होती है
✅ उत्तर: (ख) वह असीमित और कालजयी होती है
🌸 5 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों के साथ
🔷 प्रश्न 1:
कुँवर नारायण की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं?
🔶 उत्तर:
कुँवर नारायण की प्रमुख काव्य कृतियाँ –
📚 काव्य संग्रह: ‘चक्रव्यूह’ (1956), ‘परिवेश: हम-तुम’ (1961), ‘अपने सामने’ (1979), ‘कोई दूसरा नहीं’ (1993), ‘इन दिनों’ (2002), ‘हाशिए का गवाह’ (2009)
📚 खंडकाव्य: ‘आत्मजयी’ (1965), ‘वाजश्रवा के बहाने’ (2008), ‘कुमारजीव’ (2015)
💠 ‘कोई दूसरा नहीं’ के लिए उन्हें 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
🔷 प्रश्न 2:
‘बात सीधी थी पर’ कविता का मूल संदेश क्या है?
🔶 उत्तर:
➡️ इस कविता का मूल संदेश यह है कि भाषा की सहजता और सरलता ही सबसे अच्छी होती है।
➡️ जब हम कृत्रिम भाषा और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ‘बात की चूड़ी मर जाती है’।
➡️ कविता में भाषा को ‘सहूलियत से बरतने’ पर विशेष बल दिया गया है ताकि भाव स्पष्ट रूप से पहुँच सके।
🔷 प्रश्न 3:
कविता में प्रयुक्त ‘पेंच’ के रूपक का क्या अर्थ है?
🔶 उत्तर:
🔹 ‘पेंच’ का रूपक बात को समझाने की प्रक्रिया का प्रतीक है।
🔹 जिस प्रकार पेंच को सही दिशा में कसने से चीज़ मजबूत होती है, वैसे ही सही भाषा से बात मजबूत होती है।
🔹 कवि कहता है कि जब वह ‘पेंच को खोलने के बजाय बेतरह कसता चला गया’ तो इसका अर्थ है गलत तरीके से समझाने में बात उलझ गई।
🔷 प्रश्न 4:
कुँवर नारायण के काव्य की भाषा-शैली की विशेषताएँ बताइए।
🔶 उत्तर:
✳️ सरल और सहज खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग
✳️ बिंबों और प्रतीकों का कुशल प्रयोग (चिड़िया, फूल, बच्चे)
✳️ छंद मुक्त कविता
✳️ संयमित और परिष्कृत भाषा
✳️ दर्शन और चिंतन की गहराई
✳️ अनुप्रास और प्रश्नालंकार का प्रयोग
➡️ उनकी भाषा में ‘व्यर्थ का उलझाव नहीं बल्कि साफ-सुथरापन’ है।
🔷 प्रश्न 5:
‘तीसरा सप्तक’ में कुँवर नारायण का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है?
🔶 उत्तर:
📖 ‘तीसरा सप्तक’ (1959) में कुँवर नारायण का शामिल होना उनकी काव्य-प्रतिभा की पहचान थी।
📖 इसमें केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण साही के साथ वे शामिल थे।
📖 यहाँ से उन्हें ‘नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर’ के रूप में पहचान मिली।
📖 मुक्तिबोध ने उन्हें ‘अंतरात्मा की पीड़ित विवेक-चेतना और जीवन की आलोचना का कवि’ कहा था।
🌸 5 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
🔷 प्रश्न 1 (व्याख्यात्मक प्रश्न):
कुँवर नारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए।
🔶 उत्तर:
👤 व्यक्तित्व:
कुँवर नारायण (1927-2017) का जन्म फैज़ाबाद में।
🎓 लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एम.ए।
🚗 व्यवसाय: ऑटोमोबाइल (कहते थे – ‘मोटर इसलिए बेचता हूँ कि कविता न बेचनी पड़े’)।
🌸 विनम्रता, धैर्य और मध्यममार्गी विचारधारा।
📚 कृतित्व:
📖 ‘इतिहास और मिथक के जरिये वर्तमान को देखने’ की विशेषता।
📖 ‘आत्मजयी’ में कठोपनिषद, ‘वाजश्रवा के बहाने’ में वैदिक परंपरा, ‘कुमारजीव’ में बौद्ध परंपरा।
🏆 ज्ञानपीठ (2005), साहित्य अकादमी, पद्मभूषण सहित अनेक सम्मान।
🔷 प्रश्न 2 (तुलनात्मक प्रश्न):
‘कविता के बहाने’ और ‘बात सीधी थी पर’ दोनों कविताओं के मूल भाव की तुलना करें।
🔶 उत्तर:
💠 समानताएँ:
1️⃣ भाषा की शुद्धता पर बल
2️⃣ सरलता और सहजता का समर्थन
3️⃣ कविता की शक्ति का वर्णन
4️⃣ कृत्रिमता का विरोध
💠 अंतर:
🔷 ‘कविता के बहाने’ ➔ असीमित शक्ति, कालजयी प्रभाव, सर्वव्यापकता।
🔷 ‘बात सीधी थी पर’ ➔ भाषा की जटिलता और सरल भाषा की आवश्यकता।
🔷 पहली कविता ➔ आदर्शवादी दृष्टिकोण।
🔷 दूसरी कविता ➔ व्यावहारिक समस्या का चित्रण।
🔷 प्रश्न 3 (विश्लेषणात्मक प्रश्न):
कुँवर नारायण की कविता में मिथकीय चेतना का प्रयोग कैसे हुआ है?
🔶 उत्तर:
🔹 ‘आत्मजयी’ में कठोपनिषद का नचिकेता-यम संवाद।
🔹 आधुनिक मनुष्य की मृत्यु-संबंधी शाश्वत समस्या को प्रस्तुत किया।
🔹 ‘वाजश्रवा के बहाने’ में पिता वाजश्रवा की व्यथा से पीढ़ियों के बीच संवाद की समस्या।
🔹 ‘कुमारजीव’ में बौद्ध परंपरा और भाषा, अनुवाद की समस्याएँ।
🔹 उनके लिए मिथक अतीत नहीं, वर्तमान की व्याख्या का साधन।
🔹 परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु।
🔷 प्रश्न 4 (आलोचनात्मक प्रश्न):
कुँवर नारायण को ‘मध्यममार्गी कवि’ क्यों कहा जाता है? क्या यह उचित है?
🔶 उत्तर:
➡️ ‘मध्यममार्गी’ इसलिए क्योंकि उनकी कविता में अतिवाद नहीं।
➡️ न पूर्ण आदर्शवादी, न पूर्ण यथार्थवादी।
➡️ विनम्रता, संयम, परिष्कार इसका प्रमाण।
💠 यह उचित भी और आंशिक भी:
✔️ संतुलित दृष्टिकोण, सभी पक्षों की सच्चाई।
✔️ व्यक्ति की संवेदनशीलता पर बल।
❌ यह यथास्थितिवादी नहीं।
✔️ ‘अयोध्या 1992’ जैसी कविताओं में स्पष्ट रुख।
➡️ केवल ‘मध्यममार्गी’ कहना उनकी गहराई को सीमित करना।
🔷 प्रश्न 5 (समसामयिक प्रश्न):
आज के डिजिटल युग में कुँवर नारायण की ‘भाषा की सहजता’ संबंधी चिंता कितनी प्रासंगिक है?
🔶 उत्तर:
➡️ डिजिटल युग में यह चिंता अत्यंत प्रासंगिक।
➡️ सोशल मीडिया, इंटरनेट के कारण भाषा में नई समस्याएँ।
💠 समसामयिक समस्याएँ:
1️⃣ व्हाट्सऐप, ट्विटर की संक्षिप्त भाषा में भाव की हानि।
2️⃣ इमोजी, शॉर्ट फॉर्म से गहराई का ह्रास।
3️⃣ वायरल होने की चाह में कृत्रिम भाषा।
4️⃣ ट्रेंडिंग शब्दों से मूल भाव का विकृतिकरण।
💠 कुँवर नारायण का संदेश:
➡️ ‘भाषा को सहूलियत से बरतना’ आज भी ज़रूरी।
➡️ ‘बात की चूड़ी मरना’ फेक न्यूज में दिखता है।
➡️ ‘सीधी बात को सीधे कहना’ पोस्ट-ट्रुथ दुनिया में और जरूरी।
➡️ डिजिटल कम्युनिकेशन में उनका संदेश मार्गदर्शक।
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
